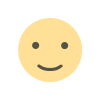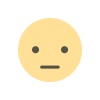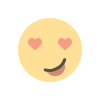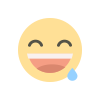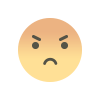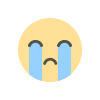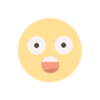क्या होता हैं डिजिटल अरेस्ट जिसके नाम पर 86 साल की महिला से की गयी 20 करोड़ की ठगी ! जानिए बचाव के उपाय

मुंबई में एक 86 वर्षीय महिला के साथ 20 करोड़ रुपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर महिला को डराया, धमकाया और इमोशनली ब्लैकमेल किया, जिससे वह लगातार तीन महीने तक ठगों के निर्देश पर बैंक ट्रांजैक्शन करती रहीं।
कैसे हुआ फ्रॉड?
यह ठगी 26 दिसंबर 2024 से 3 मार्च 2025 के बीच हुई। महिला को फोन कर बताया गया कि उनके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ है। ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया, तो उनके परिवार को भी नुकसान हो सकता है।
इसके बाद, ठगों ने महिला को "डिजिटल अरेस्ट" (Digital Arrest) के नाम पर पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया। उन्होंने फोन और इंटरनेट एक्सेस सीमित कर दिया ताकि महिला किसी से संपर्क न कर सके। इसी दौरान, उन्होंने 20 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए।
जब महिला को अहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हुई हैं, तो उन्होंने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैंक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।
ठग कैसे सफल हो जाते हैं?
हालांकि, सरकार, RBI और बैंकों के जागरूकता अभियानों के बावजूद लोग अभी भी डिजिटल अरेस्ट जैसे स्कैम के शिकार हो रहे हैं।
1. डर और धमकी का उपयोग
ठग खुद को पुलिस अधिकारी या सरकारी एजेंट बताकर पीड़ित को यह यकीन दिलाते हैं कि उनका नाम किसी अपराध में शामिल है। वे कानूनी कार्रवाई और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर पीड़ित को जल्दबाजी में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर कर देते हैं।
2. कॉलर आईडी स्पूफिंग और नकली सरकारी पहचान
ये ठग कॉलर आईडी स्पूफिंग का उपयोग करते हैं, जिससे उनका नंबर असली सरकारी नंबर की तरह दिखता है। वे फर्जी पुलिस स्टेशन का बैकग्राउंड दिखाकर वीडियो कॉल के जरिए भी भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं।
3. इमोशनल ब्लैकमेल
वे पीड़ित को यह यकीन दिलाते हैं कि अगर वे पैसे नहीं देंगे, तो उन्हें या उनके परिवार को कानूनी झंझट में फंसा दिया जाएगा। इस डर से लोग जल्दबाजी में पैसा ट्रांसफर कर देते हैं।
कैसे बचें ऐसे साइबर फ्रॉड से?
डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। अगर कोई आपको इस तरह की धमकी दे, तो इसे नजरअंदाज करें।
किसी भी अनजान कॉलर को बैंक डिटेल, आधार नंबर, OTP या कोई अन्य निजी जानकारी न दें।
अगर कोई खुद को सरकारी अधिकारी बताता है, तो उसकी पहचान अलग से वेरिफाई करें।
कॉलर आईडी स्पूफिंग से बचने के लिए सरकारी संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही नंबर चेक करें।
ऐसे किसी भी संदिग्ध कॉल को तुरंत काट दें और साइबर हेल्पलाइन (1930) या पुलिस हेल्पलाइन (112) पर शिकायत करें
यह मामला दिखाता है कि साइबर अपराधी लोगों को डर और भ्रम में डालकर कैसे लूटते हैं। सही जानकारी और जागरूकता से ही ऐसे फ्रॉड से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आए, तो घबराने की बजाय सतर्क रहें और तुरंत पुलिस में शिकायत करें।
What's Your Reaction?